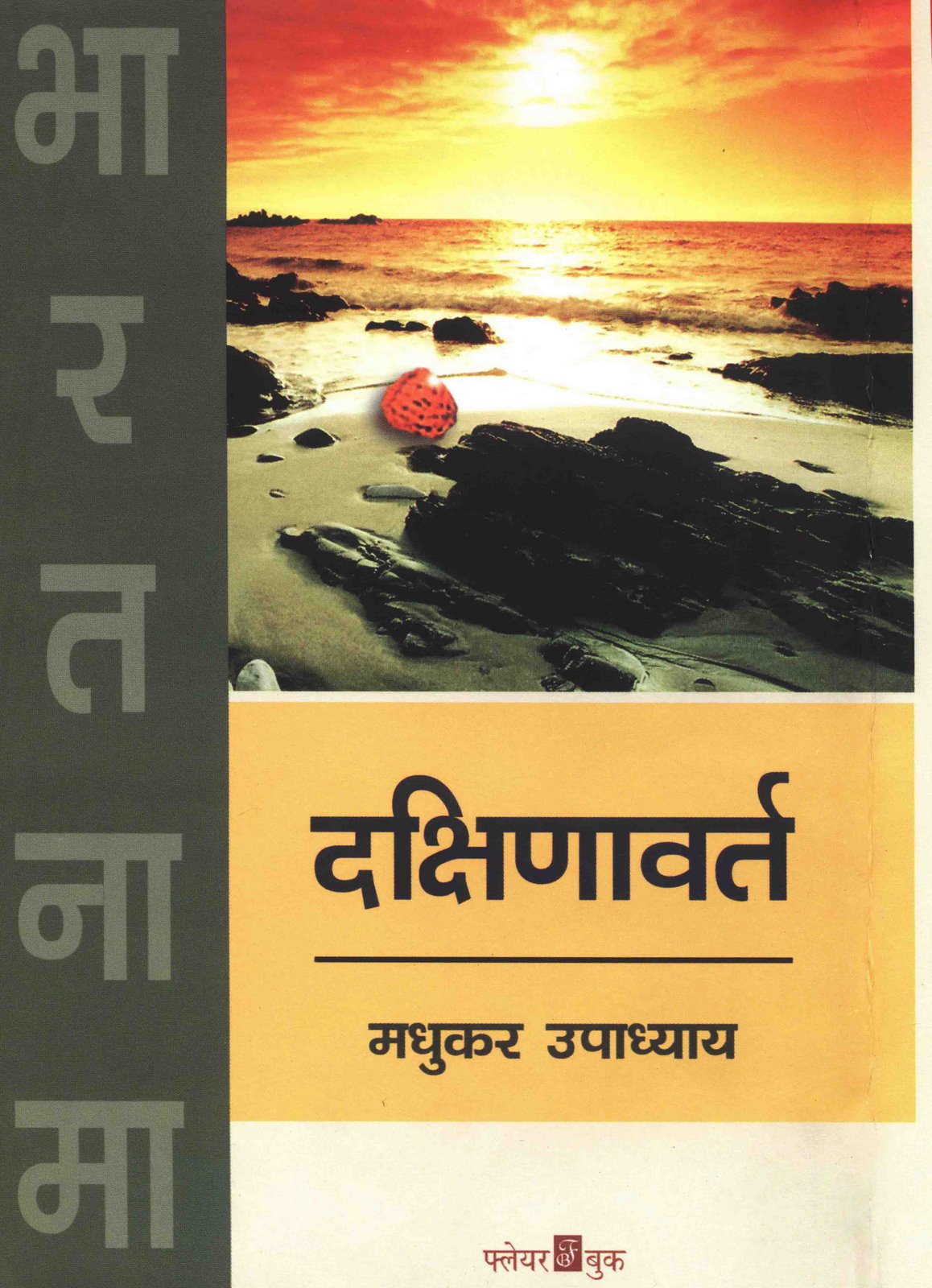Monday, March 30, 2009
कांग्रेस की कवायद
ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर अपनी मुश्किलें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। हालांकि पार्टी के कुछ नेता कहते हैं कि यह कांग्रेस की दूरगामी सोच का परिणाम है, क्योंकि वह अब से ज्यादा 2014 के बारे में सोच रही है। इस तर्क को पचा पाना आसान नहीं लगता, लेकिन जिस तरह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बिखर रहा है, इसे देखना कठिन नहीं है। कांग्रेस ने 29 जनवरी को अपनी कार्य समिति की बैठक में यह फैसला कर लिया था कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एकला चलो रे के सिद्धांत पर चुनाव लड़ेगी और अन्य राजनीतिक दलों के साथ राज्य स्तर पर सीमित समझौते किए जाएंगे।इसी निर्णय का परिणाम बिहार में लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल और राम विलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की तीन सीट लेने की शर्त न मानने के रूप में हुआ और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ उसकी मैराथन वार्ता टूट गई। तमिलनाडु में पीएमके के अलग हो जाने से कांग्रेस की हालत खराब ही होगी। एक तरह से देखा जाए, तो 543 सदस्यों की लोकसभा में कांग्रेस केवल 383 सीट पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 और तमिलनाडु तथा पुड्डुचेरी की एक सीट मिलाकर कुल 40 सीट पर उसके लिए चुनाव लड़ना, न लड़ना बराबर ही होगा। यह संख्या 160 बनती है, जहां से कांग्रेस पार्टी को बमुश्किल 10 सीट मिल सकती हैं। यह जरूर है कि कांग्रेस इन सभी सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी, लेकिन उम्मीद का दामन उम्मीदवार के हाथ शायद ही आए।कांग्रेस ने सभी 543 सीट पर एक सर्वेक्षण कराया है और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक उसे अपने तौर पर 150 सीट मिल सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि यह आंकड़ा उसे पंद्रहवीं लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि बाकी दलों की स्थिति इससे खराब रहने वाली है। निश्चित रूप से 150 सीट का यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु में उसे अपनी सही स्थिति का अंदाजा कराता है। हालांकि वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। पार्टी के सर्वेक्षण में उसे सबसे ज्यादा फायदा पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से मिलता दिखाया गया है।दरअसल 29 जनवरी की कार्य समिति की बैठक के बाद संप्रग का बिखराव अचानक बहुत तेज हो गया। जनवरी के अंत तक चट्टान की तरह संप्रग के साथ खड़ा रहने का दावा करने वाले उसके कई सहयोगी दलों में वह प्रतिबद्धता हल्की पड़ने लगी और दो महीने में पांच साल तक सरकार चलाने वाला वह संप्रग टुकड़े-टुकड़े हो गया, जिसे 2004 में संप्रग और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईंट-ईंट जोड़कर खड़ा किया था। संप्रग को बचाने या उसमें नए दलों को जोड़ने में सोनिया गांधी की तत्परता भी इस बार नजर नहीं आ रही।जनवरी के अंत के संप्रग की तस्वीर मार्च के अंत तक इतनी बदल गई कि उसकी पहचान भी मुश्किल हो गई। कुछ छोटे दलों और समूहों को छोड़ दिया जाए, तो संप्रग से किनारा करने वाले दलों की संख्या उसके साथ टिके रहने वाली पार्टियों से चार गुना ज्यादा है। यह केवल उत्तर या दक्षिण तक सीमित नहीं है, इसका असर चौतरफा हुआ है। संप्रग से हटने या चुनावी जंग में किनाराकशी करने वाले दलों में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, पीडीपी, एमडीएमके, पीएमके और तेलंगाना राष्ट्र समिति शामिल है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना होगा। उसके साथ बचे दलों में मुख्य रूप से केवल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और डीएमके का नाम लिया जा सकता है।सवाल यह उठता है कि आखिर 29 जनवरी की कार्य समिति की बैठक में संप्रग के बिखराव की आशंका व्यक्त किए जाने के बावजूद पार्टी ने सहयोगी दलों को नाराज करने की हद तक जाकर ऐसा फैसला क्यों किया कि वह अधिकतर सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस निर्णय में 2009 के चुनाव की तात्कालिकता नहीं थी, लेकिन पार्टी ने इसे भविष्य के बारे में सोचते हुए कड़वी दवा की तरह पीने का फैसला किया।कार्य समिति में यह बात भी सामने आई कि कांग्रेस को बचाए रखने के लिए जरूरत होने पर पार्टी को अन्य विकल्पों के साथ विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी ने इसे पराजय की मानसिकता की जगह भविष्य दृष्टि के रूप में देखने की दलील दी। इससे तो यही लगता है कि उसकी नजर 2009 पर नहीं, बल्कि उसके आगे है। लालू यादव ने इस संबंध में टिप्पणी की थी कि पार्टी 2009 का चुनाव नहीं लड़ रही, 2014 की तैयारी कर रही है।एक तरह से देखा जाए, तो शायद गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ने और क्षेत्रीय दलों की इनायत पर तीन या पांच सीट लेने पर अगले चुनाव तक कांग्रेस का कम से कम उत्तर भारत से पूरी तरह सफाया हो जाता। पार्टी ने संभवत: इसीलिए जीत से ज्यादा महत्व मौजूदगी को दिया। आजाद भारत के 60 में से लगभग 50 वर्ष सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए यह फैसला आसान नहीं रहा होगा। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर कांग्रेस ने यह निर्णय न किया होता, तो बतौर राष्ट्रीय पार्टी, यह उसका आखिरी चुनाव होता।
Subscribe to:
Posts (Atom)